अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ – anterrashtriya vyapar ka arth
जब हम दो राष्ट्रों के बीच में वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान – प्रदान करने को अन्तराष्ट्रीय व्यापार कहते है। अन्तराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य है स्थानीय जरूरतों की पूर्ति करना और लाभ कमाना होता है। अन्तराष्ट्रीय व्यापार के दो घटक होते है 1) आयात तथा 2) निर्यात
1) निर्यात – जब हम वस्तुओं को दूसरे देशों में लाभ के उद्देश्य से भेजते है तो इसे निर्यात कहते है।
2) आयात – जब हम जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरें देशों से वस्तुओं को मँगाते है। तो उसे आयात कहते है।
antarrashtriy vyapar ke mahatva
अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्व
1) भौगोलिक श्रम –
विभाजन या अलग – अलग होने के कारण विश्व के विभिन्न देश सभी वस्तुओं का उत्पादन करने में समान रूप से कुशल नहीं है। अन्तराष्ट्रीय व्यापार के कारण ही जब भौगोलिक श्रम- विभाजन और विशिष्टिकरण सम्भव होता है। तो सभी देश उन वस्तुओं का उत्पादन करते है जो उनकी भौगोलिक तथा आर्थिक परिस्थितियॉ के अनुकूलतम होता है। इस प्रकार से साधनों का उत्तम उपयोग होता है। और सभी देशों में वास्तविक आय तथा जीवन - स्तर को बढ़ाने में सहायता मिलती है।
2) वस्तुओं की कीमतों में समानता -
यातायात खर्चा तथा सीमा कर आदि की रूकावटों के कारण विभिन्न देशों में वस्तुओं की जो कीमतें होती है वह एक समान नहीं हो पाती है। और इन रूकावटों को दूर करने के लिए लागत के बराबर अन्तर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतो में अन्तर होता है, परन्तु फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न देशों के उत्पादकों की परस्तर प्रतियोगिता का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव वस्तुओं की कीमतों या मूल्य में समानता की प्रवृति स्थापित करना होता है।
3) उपभोक्ता को लाभ -
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही उपभोक्ता को बहुत सी अनेक वस्तुऍं के उपलब्ध होती है। जिनका वस्तुओ का उत्पादन उसके देश में नहीं होता है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उपभोग के क्षेत्र को विस्तृत करने करने में सहातक होता है। इतना ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के कारण किसी एक देश की सामान्यत: वस्तुओं की मूल्यों बहुत अधिक नहीं बढ़ पाती है। क्योंकि एकाधिकार व्यवसाय नहीं शुरू हो पाते है।
4)आर्थिक विकास में सहयोग -
औद्योगिक विकास के लिए किसी भी देश अन्य और देशों पर निर्भर रहता पड़ता है। उत्पादन के लिए मशीनें आदि इस अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मध्य से प्राप्त होती है। और इस कारण से ही यह बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। उत्पादन अपनी वस्तुओं का बाजार में विस्तृत रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से ही वस्तुओ की उत्पादन की विधियों और तकनीकों में सुधार करने के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहता है। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बिना वर्तमान औद्योगिक संगठन सम्भव नहीं हो पाता हैा और आधुनिक औद्योगिक समाज की स्थापना होना असम्भव होता है।
5)कच्चे मान की प्राप्ति -
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश के अतिरिक्त साधन तथा कच्चा मान उन देशों को पहुचाता है जिनको अपने उद्योगों को चलाने की जरूरत हि नहीं पडती हैा यदि ब्रिटेन को अन्य देशों से कच्चा माल न मिलता तो वह इतना औद्योगिक विकास नहीं कर सकता था किसी भी देश के साधनों का उचित उपयोग करने में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ज्यादा सहायक होता है।
6)संकटकाल में सहायक होना -
किसी भी देश पर प्राकृतिक आपदा या कि अन्य प्रकार के संकट पड़ने की स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण अन्य देशें से उन वस्तुओं का आयात कर किया जाता है जिनकी संकटग्रस्त देश में जरूरत होती है। अकालों को कम करने का बहुत कुछ श्रेय अर्न्राष्ट्रीय व्यापार को ही जाता है।






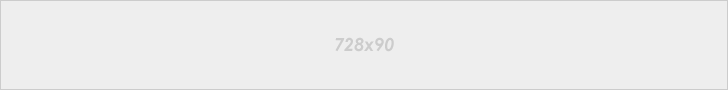
No comments:
Post a Comment